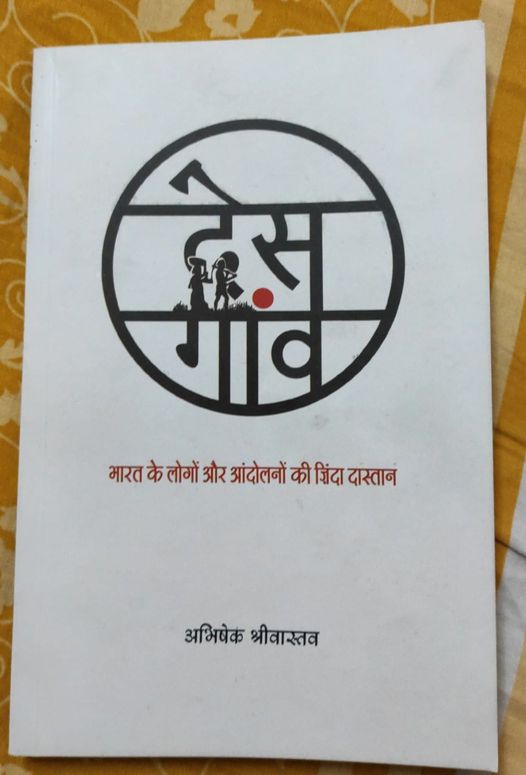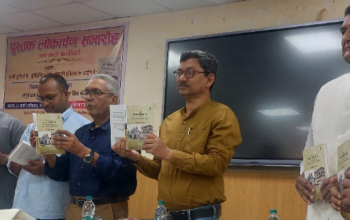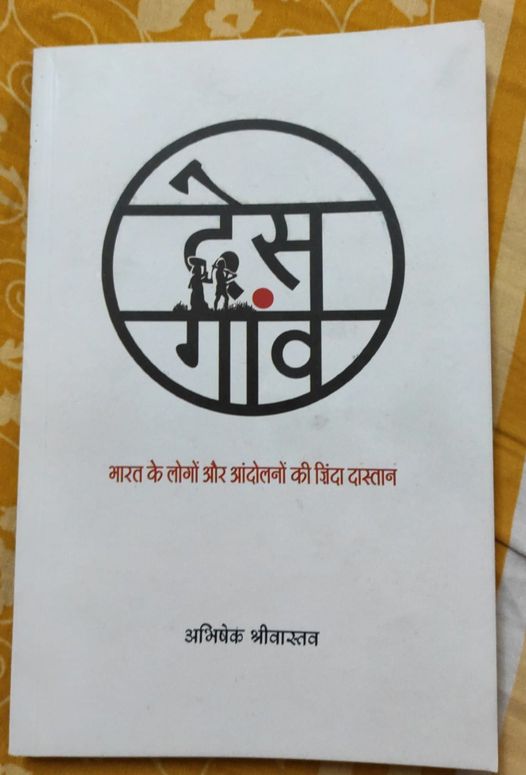
प्रिय दर्शन
हिंदी पत्रकारिता में पिछले कुछ वर्षों में छिछलापन लगातार बढ़ा है। अब न वैसे बौद्धिक संपादक बचे हैं जिन्हें अपने पाठकों को अच्छी सामग्री देने की चाहत हो और न ही ऐसे संवेदनशील रिपोर्टर जिनके पास वैचारिक समझ और उसे रखने लायक भाषा हो। आज की तारीख़ में हिंदी अखबार पढ़ना अमूमन कोफ्त और व्यर्थता-बोध से गुज़रना है। उसमें पेशेवर धार पूरी तरह ग़ायब है और सतही व्यावसायिकता हावी है। मुख्यधारा की पत्रकारिता के समानांतर जो प्रतिबद्ध क़िस्म के निजी मीडिया-उपक्रम हैं उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वे किसी को कहीं भेज कर ज़मीनी रिपोर्ट मंगवा सकें। ऐसे में रिपोर्टिंग कुछ सामाजिक संस्थाओं या गैरसरकारी संगठनों के बुलावे पर की गई किसी यात्रा की मोहताज रह जाती है या फिर कुछ स्थानीय संपर्कों से ली गई आधी-अधूरी जानकारियों पर आधारित ऐसा ब्योरा, जिससे कोई मुकम्मिल तस्वीर बनाना आसान नहीं होता। कुल मिलाकर हिंदी पत्रकारिता में अच्छी रिपोर्ट पढ़ने का सुख जाता रहा है।
इस सूखे के बीच और इन सीमाओं के बावजूद अगोरा प्रकाशन से आई अभिषेक श्रीवास्तव की किताब ‘देस गांव’ को पढ़ने का अपना सुख है। अभिषेक ने बीते एक दशक के दौरान अलग-अलग जगहों पर चल रहे जनांदोलनों के बीच जाकर जो रपटें तैयार की हैं, यह किताब उन्हीं का संचयन है। अभिषेक के पास साफ़-पैनी दृष्टि है और सघन-समर्थ भाषा-बेशक वह सरोकार तो है ही जिसकी वजह से वे इन इलाकों में गए और उन्होंने वहां की खबरें लिखीं। किताब का कैनवास बड़ा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, गुजरात राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक के अलग-अलग क्षेत्रों की ये रपटें एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं लेकिन इनके बीच एक-दूसरे को जोड़ने वाली एक बहुत स्पष्ट अंतर्कथा है जिसका वास्ता भारत में विकास के नाम पर चल रही परियोजनाओं से पैदा हो रही एक जैसी विडंबनाओं से है।

ये रपटें बताती हैं भारतीय राष्ट्र राज्य में सत्ता कैसे निरंकुश हुई है, दलाल एजेंसियां किस क़दर बेलगाम हैं और जनता कैसे पिस रही है। विकास नाम की गाय ताकतवर लोगों के आंगन में बंधी हुई है और इसके विरुद्ध बोलना कुफ़्र है और जनांदोलन करना अपराध। किताब सोनभद्र में कनहर बांध के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस दमन और गोलीबारी के ज़िक्र से शुरू होती है। यह 2015 का वाकया है। मुख्यधारा के मीडिया में यह ख़बर सिरे से ग़ायब है। इस मामले की जांच के लिए एक टीम इलाक़े में जाती है तो लगातार उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। लगता है, जैसे पुलिस इस टीम को गिरफ़्तार ही कर लेगी। यह पूरी रिपोर्ट बताती है कि भारतीय राष्ट्र राज्य अपने नागरिकों के साथ किस छल-बल से पेश आ रहा है। लेकिन यह मामला इतना सपाट भी नहीं है। अभिषेक यह भी पाते हैं कि दरअसल मामला सीधे-सपाट आंदोलन और दमन तक सीमित नहीं है, उसमें जातिगत बाड़ेबंदियों की सड़ांध है, राजनीतिक घेराबंदियों का सयानापन है, अफ़सरों और दलालों का काइयांपन है, एनजीओ सेक्टर की हिस्सेदारी है, संस्थाओं के आपसी टकराव हैं और कुल मिलाकर ऐसा कुहासे वाला माहौल है जिसमें कुछ भी साफ़-साफ़ देखना बहुत आसान नहीं है।
यह कहानी जैसे पूरी किताब में पसरी है। इसकी जगहें बदलती जाती हैं, मुद्दे भी बदलते हैं, किरदार भी बदलते हैं, लेकिन मूल कथा वही रहती है। कहीं गंगा की बाढ़ में डूबी ज़मीन के मुआवज़े के नाम पर हो रहा तमाशा है तो कहीं दलित उत्पीड़न की त्रासदी है, कहीं अकाल और दुष्काल की वह ठहरी हुई कहानी है जिसे राजनीति अपने-अपने ढंग से इस्तेमाल करने में लगी है। किताब में नर्मदा में हुए जल सत्याग्रह से जुड़ी अंदरूनी रपटें भी हैं और ओडिशा के नियामगिरि के इलाक़े की वह खदबदाहट भी जिसमें कभी वेदांता की एक परियोजना को स्थानीय पंचायतों ने मिलकर नकार दिया था। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान जैसे राज्यों में अलग-अलग मुद्दों पर चल रहे दमन और आंदोलन की रपटें भी इसमें हैं।

बेशक, अलग-अलग समय की ऐसी अलग-अलग रिपोर्ट पढ़ते हुए किसी आंदोलन को समझने की पूरी तसल्ली नहीं मिलती, फिर यह जानने की इच्छा भी बची रहती है कि आने वाले दिनों में वहां क्या हुआ, लेकिन अगर कोई किताब आपको यहां तक भी ले आए कि आप इन मुद्दों पर विचार करने को मजबूर हों तो यह छोटी उपलब्धि नहीं। सबसे बड़ी बात- पूरी किताब से गुज़रते भारतीय राष्ट्र राज्य का एक अक्षम चेहरा उभरता है जो इस अक्षमता को छुपाने के लिए लगातार क्रूर हुआ जाता है। हाल के वर्षो की सांप्रदायिकता और उसके एजेंट इस क्रूरता और इसके छल में इजाफऱा ही करते हैं। वे आंदोलनों में सेंधमारी करने और पलीता लगाने का उपक्रम भी करते दिखाई पड़ते हैं।
निस्संदेह, किताब में कहीं-कहीं संपादकीय असावधानियां भी हैं। ‘पचास साल की नाइंसाफ़ी और शर्म’ का अध्याय इसके पहले के लेख में लगभग दुहरा दिया गया है। इसी तरह एक लेख में ‘मीडिया विजिल’ द्वारा लिखा गया इंट्रो भी चला गया है जिसे संपादित करने की ज़रूरत थी। पत्थरगड़ी का ज़िक्र है, लेकिन राजस्थान के हवाले से, जबकि इसको लेकर झारखंड में चले आंदोलन का क़रीने से ज़िक्र नहीं है।लेकिन इन छोटी-मोटी शिकायतों के बावजूद यह एक ज़रूरी किताब है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। अभिषेक कई बार भाषा के लालित्य में फंसते हैं (यह दोष इस लेखक का भी है), कई बार बतकही में भटकते भी हैं, लेकिन इन सबके बावजूद वे एक चौकन्ने और ज़रूरी लेखक हैं- यह बात इस किताब से पहले उनकी टिप्पणियां साबित करती रही हैं।
भारतीय राष्ट्र राज्य के कोनों-अंतरों में विकास के छल, सत्ता के दमन और इसके विरुद्ध जनता के प्रतिरोध की कहानियां बताने वाली मौलिक किताबें हिंदी में तत्काल याद नहीं आतीं- इस लिहाज से यह किताब अभिषेक की ओर से एक ज़रूरी और सामयिक हस्तक्षेप है- वह भी ऐसे समय, जब सतही विकास, खोखले ऱाष्ट्रवाद और खूंखार सांप्रदायिकता का गठजोड़ सबकुछ ढंक लेने पर आमादा है। उनको इस किताब के लिए बधाई।
वरिष्ठ पत्रकार प्रिय दर्शन के फेसबुक बॉल से साभार