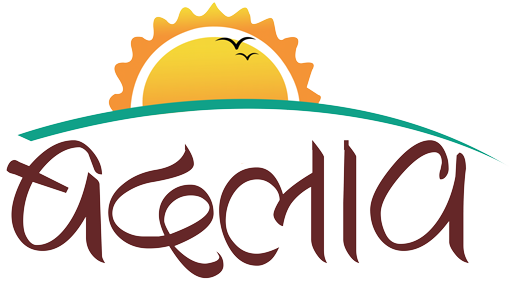शिरीष खरे
आज मैं फिर जल्दी जागा हूं, फटाफट नहाकर और तैयार होकर एक बार फिर सुबह छह बजे के पहले होटल से बाहर आने में सफल रहा हूं। लेकिन, सूरज शेडलीवार मुझसे भी पहले तैयार होकर होटल के सामने वाली सड़क पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेलघाट में इतने अनुशासित साथी पाकर मैं धन्य हूं! खैर, सूरज की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर मैं उसके साथ आज एक नई दिशा की ओर निकल पड़ा हूं, लेकिन इस दिशा की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है। वजह है कि चिखलदरा से महज तीन किलोमीटर दूर भीमकुंड नाम से एक दर्शनीय स्थल है, जहां हमारे साथ और हमसे पहले बहुत सारे पर्यटक सुबह का आनंद उठाने पहुंच गए हैं। यहां 3,500 फीट की गहरी खाई और एक भव्य झरना है, दूर तक पहाड़ी जंगल नजर आता है। प्रकृति के हरे, सफेद, कत्थई रंगों के बीच रजत आसमान में सोने जैसा चमकता सूरज सबका ध्यान खींच रहा है। लेकिन, फिर भी आज का सूरज मुझे कल की अपेक्षा थोड़ा कम चमकदार लग रहा है। यहां आने वाले पर्यटक नजदीक ही दूसरे दर्शनीय स्थल गाविडगड का किला देखने जरुर जाते हैं।
आईने में अपना अक्स-पांच
भीमकुंड के मिथक और गाविडगड के किले के इतिहास के बारे में सूरज ने मुझे कई बातें बताईं। लेकिन, आसपास आदिवासियों की जिंदगी के चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देते। मेलघाट में 80 प्रतिशत कोरकू आदिवासी होने के बावजूद उनका जीता जागता संसार मानो यहां से दूर-दूर तक विस्थापित कर दिया गया हो। मैं नहीं जानता हूं कि कोरकू बोली में ‘मिथक’, ‘अतीत’ या ‘भविष्य’ के लिए कौन-से शब्द प्रचलित हैं, मुझे तो हिन्दी भाषा में उनसे उनके वर्तमान के बारे में जानना है। और इन पर्यटकों में एक भी आदिवासी दिखाई नहीं देता, जिससे जंगल के भीतर की दुनिया के बारे में पूछा जा सके। लिहाजा, जल्द ही हम यहां से ठीक विपरीत दिशा की ओर बिना देर किए निकल पड़ते हैं। हालांकि, भीमकुंड के दक्षिणी दिशा की ओर 150 से 1,500 फीट गहरे कई जलकुंड हैं, छोटे-छोटे झरने हैं, यही वजह है कि एक ओर विदर्भ सूखा क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेलघाट की तस्वीर पानीदार पहाड़ियों के रूप में उजागर होती है। लेकिन, हमारी मोटरसाइकिल दौड़ रही है इस तस्वीर के ठीक उलटी दिशा में, जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कई गांव पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे होंगे।
माखला पानी के लिए तरसते गांवों में से एक गांव है। यहां बस्ती के रास्ते पांच-छह महिलाएं सिर पर स्टील के तीन-चार बर्तनों को एक के ऊपर एक साधे चल रही हैं। उनके पीछे बच्चे साइकिल के टायर चलाते हुए नंगे पैर चल रहे हैं।
-”आप पानी लेने के लिए कहां जा रही हैं?”-”पहाड़ियों पर, दो किलोमीटर दूर।”-”क्यों, आसपास में कोई हैंडपंप नहीं है?”-”नहीं है, पीने का पानी (पहाड़ियों से) चढ़कर लाते हैं।”
हम भीमकुंड से पचास किलोमीटर दूर आ गए हैं, यहां परिवार के सदस्यों की प्यास बुझाने की पहली जिम्मेदारी महिलाओं के सिर पर है। इनके साथ पहाड़ियों की तरफ चलते हुए बातचीत की तो जाना कि यह तो इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह जल्दी उठना और पानी भरने के लिए हर रोज डेढ़-दो किलोमीटर जाना और लौटना एक सामान्य बात है। मीना (परिवर्तित नाम) जैसी महिलाओं के घर में छह से सात जन हैं, इसलिए इन्हें पानी के लिए दो बार चक्कर लगाना ही पड़ता है।
एक घर के सामने बिना बैलों की गाड़ी पर नीली प्लास्टिक की बड़ी टंकी रखी है, झांककर देखता हूं तो उसमें चार-पांच बाल्टी ही पानी है। मखाला करीब ढाई सौ घरों और हजार आबादी का बसा छोटा गांव है। इसके आस-पास की वीरानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मखाला का निकटतम बड़ा गांव सेमादोह यहां से दस किलामीटर दूर है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में बिजली नहीं है, लेकिन पानी की कमी इन्हें सबसे ज्यादा सताती है। हालांकि, यह बाघ संरक्षण परियोजना से प्रभावित गांव नहीं है, इसके बावजूद लोग पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं।
और फिर शाम से ठीक पहले चिखलदरा से अपने ठिकाने की ओर लौटते हुए हमने एक बात नोटिस की, इस मार्ग पर वाकई इतना सन्नाटा है कि सेमादोह को छोड़कर कहीं ढंग का भोजनालय भी नहीं दिखा। एक जगह चाय पीने बैठे तो और एक बात ध्यान आई, हमने ज्यादातर लोगों को अपने सिर पर कुछ न कुछ बोझा लादे देखा है। किसी के सिर पर पानी के बर्तन, किसी के सिर पर यात्रा के बैग, किसी के सिर पर बाजार के थैले, छोटे बच्चों के सिर पर छोटे थैले, बुजुर्गों के सिर पर टोकरियां, युवकों के सिर पर तगाड़ियां। यदि कोई थककर लेटा भी है तो इन्हीं बैगों, थैलों, टोकरियों, तगाड़ियों को सिर टिकाने का सहारा बनाकर।
”पैसे देकर हमने सबसे पहले नमक खरीदा था! बचपन में मैंने दुकान नहीं देखी थी।”
इतना बोलते ही झोलेमुक्का धाण्डेकर फिर चुप हो गए। बागलिंगा गांव के धाण्डेकर अपनी उम्र के 85 बरस पार कर चुके हैं। लोग बताते हैं कि ये यहां के सबसे बुजुर्ग और जानकार आदमी हैं। हम उनकी छोटी और सुंदर झोपड़ी के भीतर उन्हीं के साथ नीचे बोरे पर बैठे हैं। यह उम्र का असर है या उनके व्यक्त्त्वि का, जो उनके चेहरे पर मासूम बच्चों से भी ज्यादा मासूमियत है। कुछ पूछने पर थोड़ा-सा बोलकर चुप हो जाते हैं। आवाज महिलाओं जैसी पतली और बातें विशुद्ध कोरकू बोली में, मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। इसलिए, मेरे साथ आए कालूराम बेलसरे ही उनसे पूछ रहा है और उनकी कही हर बात को मुझे हिन्दी में लिखवा रहा है।
-”बाबा, तब भी क्या पंचायत होती थी, कायदा (कानून) बनता था?”-”साल में सब एक बार बैठते थे, ‘भवई’ (त्यौहार) पर। तब सालभर का कामकाज बांटा जाता था, मिलकर कायदा बनाते थे।”-”बैठक में महिलाएं होती थीं!…शादियां कैसे होती थीं?”-”हां, ‘भवई’ के दिन वे भी बैठती थीं, वे अपनी मर्जी से दूसरी, तीसरी या उससे भी अधिक बार शादी कर सकती थीं।”
 घर के भीतर बहुत अंधेरा है, इसलिए लिखने में दिक्कत होने के कारण हम उनसे बाहर बैठने की गुजारिश करते हैं। फिर तीनों खुली दलान पर बोरा बिछाकर बैठते हैं। धाण्डेकर गांव की ओर देखते हुए पहली बार खुद से बोलते हैं, ”हमारी बस्ती पेड़ों से घिरी थी। सागौन, हल्दू, साजड़, बेहड़, तेंदू, कोसिम, सबय, मोहिम, धावड़ा, तीवस, कोहा से।” बागलिंगा कोई 800 लोगों की आबादी वाला गांव है, जो चिखलदरा से 35 किलोमीटर दूर पक्की सड़क पर है।
घर के भीतर बहुत अंधेरा है, इसलिए लिखने में दिक्कत होने के कारण हम उनसे बाहर बैठने की गुजारिश करते हैं। फिर तीनों खुली दलान पर बोरा बिछाकर बैठते हैं। धाण्डेकर गांव की ओर देखते हुए पहली बार खुद से बोलते हैं, ”हमारी बस्ती पेड़ों से घिरी थी। सागौन, हल्दू, साजड़, बेहड़, तेंदू, कोसिम, सबय, मोहिम, धावड़ा, तीवस, कोहा से।” बागलिंगा कोई 800 लोगों की आबादी वाला गांव है, जो चिखलदरा से 35 किलोमीटर दूर पक्की सड़क पर है।-”बाबा, आपने अंग्रेजों का जमाना देखा है। क्या वे आपको तंग करते थे?”-”वे हमसे लकड़ियां कटवाते थे। वे तंग नहीं करते थे। जंगल में आग लगती थी तो हम ही बुझाते थे, इसलिए (जंगल में) वे रहने देते थे। जंगल में किसी चीज के इस्तेमाल की मनाही नहीं थी।”
कालूराम बाबा को पुरानी साग-सब्जियों, दालों, छालों और फलों के नाम लिखवाने के लिए तैयार करता है। वे रुक-रुक कर बताते हैं और हम लिखते जाते हैं। वे बताते हैं कि उनके जमाने में सालगिरी, गालंगा और आरा की भाजियां थीं, जो अब कम ही खाई जाती हैं। बेचंदी को चावल की तरह उबालकर खाते थे। काला गदालू, बैलकंद, गोगदू और बाबरा कच्ची खाई जाने वाली चीजें खूब मिलती थीं। ज्वास नाम की बूटी को उबली सब्जी में डाल दो तो वह तेल की तरह काम करती। इसी तरह, तेंदू, आंवला, महुआ, हिरडा जैसे फलों के पेड़ ही पेड़ थे। खेती के लिए कोदो, कुटकी, जगनी, भल्ली, राठी, बड़ा आमतरी, गड़मल और सुकड़ी के बीज थे, जो बंजर जमीन पर भी उग जाते थे।
इतनी सारी जानकारियां हासिल करने के बाद धाण्डेकर के चेहरे पर मुझे कोरकू समुदाय की सरल, सहज और समृद्ध जीवनशैली की झलक दिखाई दी। इन्होंने जंगल से जीवन को जीना सीखा था, लेकिन जैसे-जैसे जंगल से उनके जीवन को अलग-थलग किया गया और वैसे-वैसे इनका जीवन दूभर होता चला गया।
 मेलघाट , 1974। ठीक से 100 तक गिनती न आने के बावजूद मेलघाट में वर्ष 1974 कई बड़े-बूढ़ों की जुबान पर है, क्योंकि इसी वर्ष ‘मेलघाट टाइगर रिजर्व’ वजूद में आया और कोरकू जनजाति का जीवन दो टुकड़ों में बट गया-विस्थापन और पुनर्वास। ऊंट के आकार में फैले विस्थापन के सामने पुनर्वास जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ। आजाद भारत में कोरकू जनजाति पर एक के बाद एक कई प्रहार हुए और इनका जीवन जंगल से कटता गया।
मेलघाट , 1974। ठीक से 100 तक गिनती न आने के बावजूद मेलघाट में वर्ष 1974 कई बड़े-बूढ़ों की जुबान पर है, क्योंकि इसी वर्ष ‘मेलघाट टाइगर रिजर्व’ वजूद में आया और कोरकू जनजाति का जीवन दो टुकड़ों में बट गया-विस्थापन और पुनर्वास। ऊंट के आकार में फैले विस्थापन के सामने पुनर्वास जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ। आजाद भारत में कोरकू जनजाति पर एक के बाद एक कई प्रहार हुए और इनका जीवन जंगल से कटता गया।”1974 में (तत्कालीन) प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थीं, वे कोलकस रेस्टहाउस में ठहरी थीं, उस समय रामू पटेल प्रदेश के वनमंत्री थे, उन्होंने कुछ खास लोगों को रेस्टहाउस बुलवाया था। कहा था, सरकार बाघों को बचाना चाहती है, इसलिए मेलघाट में बाघों के चमड़े बराबर जगह चाहिए और आज आप देख ही रहे हैं कि बाघ का चमड़ा कैसे चौड़ा होते-होते पूरे मेलघाट को ढकने लगा है।”
वैराट गांव के ठाकुजी खड़के जब यह सब बता रहे हैं तो मुझे यात्रा के दौरान टाइगर रिजर्व परियोजना के कुछ बोर्ड याद आते हैं, जिन पर मराठी भाषा में कई संदेश लिखे गए। इन्हीं पर एक बोर्ड पर लिखा था, ‘बाघ पर्यावरणाचे प्रतीक आहे’ अर्थात बाघ अच्छे पर्यावरण के प्रतीक हैं। मैं सोचता हूं कि क्या जंगलों में आदिवासियों का होना भी अच्छे पर्यावरण का प्रतीक नहीं समझा जा सकता! बीते चार दिनों में मैंने देखा कि वन्यजीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग आदिवासियों से बतियाते हैं! दरअसल, देश जंगल के भीतर बनाम जंगल के बाहर की दुनिया में विभाजित है। जंगल के भीतर की दुनिया में भले ही टाइगर सुरक्षित हो रहा हो, लेकिन यहां लोगों की रोटी का संकट जरूर गहराता जा रहा है। जंगल के बाहर की दुनिया इस बात से अनजान है, या उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि बीते तीन दशकों से यहां जनजातियों का ही शिकार जारी है।
और इसी कड़ी में अब वैराट और पसतलई जैसे गांवों पर विस्थापन की तलवार लटका दी गई है। चिखलदरा से महज दस किलोमीटर की दूरी पर एक-दूसरे से सटे ये दो छोट-छोटे गांव हैं, जबकि यह घूमते समय मुझे लगा कि ये एक ही गांव की दो बस्तियां होंगी। दोनों गांवों के कुल 95 घरों में करीब पांच सौ लोग रहते हैं। ”1974 के पांच-छह साल बाद सरकार ने जल से मछली, जंगल से पेड़ों की पत्तियां और जमीन से कंदमूल खोदने पर रोक लगा दी। 1974 के बाद से जब अफसर फाइल लेकर इधर-उधर घूमते तो हमने सोचा नहीं था कि एक दिन वे हमें जंगलों से इस तरह अलग कर देंगे। वे जीपों से आते और कहते तुम्हें घर और खेती के लिए जमीन दी जाएगी। हमें अचरज होता कि जो जमीन हमारी ही है, उसे वे क्यों देंगे!”
दरअसल, पसतलई गांव के तुकाराम सनवरे का यह बयान जंगल के मालिकों को मजदूर बनाने की लघुकथा है। मनरेगा के तहत मेलघाट की पहाड़ियों से 46 हजार लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं।
”जिंदाबाद!” कई लोगों ने एक जगह से मिलकर यह नारा लगाया। मैं खुश हूं, बल्कि गदगद हूं, यह देखकर कि वैराट गांव में एक घर की लंबी और खुली दलान पर वैराट और पसतलई गांव के लोगों ने मेरे यहां आने की सूचना पर बैठक रखी है। पचास से ज्यादा लोग और खास तौर से महिलाएं अपने-अपने काम छोड़कर यहां क्या सोचकर बैठी हैं! मैं इनके बारे में बात करने के लिए आने वाला कोई पहला पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं हूं! फिर कालूराम मुझे बताता है कि ये बाहर से आए व्यक्तियों का इसी तरह से स्वागत और सम्मान करते हैं। ‘जिंदाबाद’ के जवाब में मेरा एक हाथ अपने आप ही उठ गया, भीतर ही भीतर यह सोचकर कि न मैं मंत्री हूं और न अफसर, जो मेरे लिखे से इनकी तकदीर बदल जाएगी! फिर भी इनकी उम्मीद और इनका प्यार मेरी जिंदगी की पूंजी है। यह सच्चाई है कि कोरकू समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस तरह के समुदायों के सामने आकर मुझे मेरी पहचान हासिल होती है, वरना मेरी दुनिया में तो मुझमें कोई बात नहीं है। मेरी दुनिया से अलग इस दुनिया के लोग हर बार पूरे अनुशासन और ध्यान से मेरी बातें सुनते और अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन इस दुनिया से बाहर जब यहीं बातें मैं सुनाता हूं तो कौन सुनता है! मैं खुद इनकी तरह ही वंचित हूं, ये व्यवस्था से वंचित हैं और मैं अपने पेशे से।
चर्चा शुरू होती है तो मुझे पता चलता है कि मेलघाट में इसके पहले तीन गांव कोहा, कुण्ड और बोरी के 1,200 घरों को विस्थापित किया जा चुका है, पुनर्वास के नाम पर उन्हें यहां से 120 किलोमीटर दूर अकोला जिले के अकोट तहसील क्षेत्र में राजूरा गांव के पास बसाया जा चुका है। कालूराम खड़े होकर बता रहे हैं कि शिरीष भाई ने उन तीन गांवों का पुनर्वास नहीं देखा। वे लोगों से पूछ रहे हैं कि उन तीन गांवों का पुनर्वास कैसे हुआ और क्या वे भी उसी तरह से बसना चाहते हैं?
”नहीं, नहीं” सभी एक सुर में पुनर्वास का विरोध कर रहे हैं। तेजुजी सनवारे कहते हैं, ”अफसर ठीक से सर्वे नहीं करते। कागज और जमीन पर फर्क होता है। कुण्ड गांव के ही छह परिवार ऐसे हैं जिन्हें खेती के लिए जो जमीन बताई गई थी वह तालाब के भीतर पाई गई। फिर, कई लोगों को अपने जानवर बेचने पड़े, क्योंकि वहां चराने के लिए जमीन नहीं थी।” फकीरजी खड़के कहते हैं, ”हम मरने के बाद आदमी को जमीन के नीचे दफनाते हैं। वहां दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो हम कहां जाएंगे।” किशन खड़के बताते हैं, ”वहां गए कुण्ड के 11 परिवारों को सरकार ने न घर बनाने के लिए पैसा दिया, न जमीन दी।”
सुखदेव एवले बताते हैं, ”बस्तियां तोड़ने से पहले अफसर आते हैं और बताते हैं कि बस अब इतने दिन और बचे हैं, फिर तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। अफसर के आने का मतलब है कोई खतरा आ गया।” शांता सनवारे कहती हैं, ”बस्तियों को तोड़ने का उनका तरीका ही अजब है। जिस बस्ती के आसपास आठ-पंद्रह दिन पहले ट्रक घूमने लगें, समझो घर-गृहस्थी समेटने का समय आ गया। घर तोड़ने वाले कर्मचारी चाय की दुकानों पर चर्चा करते हैं कि पूरी बस्ती को वे किस तरह तोड़ेंगे!”
फूलाबाई खड़के आगे जोड़ती हैं, ”वे (कर्मचारी) कहते हैं, बंबई से चला तीर लौटता नहीं है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही, समय रहते चले गए तो कुछ मिल ही जाएगा, नहीं तो घर की लकड़ियां, खपड़े और ईंट निकालने का समय भी नहीं देंगे। ऐसी बातों को सुनकर जब हमारे बच्चे अपने घरों की लकड़ियां निकालने लगते हैं तो वे हमारे बच्चों को शाबाशी देते हैं और बस्ती तुड़वाने में हमारी मदद करते हैं। फिर देखते ही देखते गांव की पूरी बस्ती के घर टूट जाते हैं।”
यह कहानी है कोहा, कुण्ड और बोरी गांवों के उजड़ने की, जहां के बाशिंदे मेरे आने के सात साल पहले उजड़ गए।
जो तिनका-तिनका जोड़कर
जिंदगी बुनते थे
वो बिखर गए।
गांव-गांव टूट-टूटकर
ठांव-ठांव हो गए।
अब उम्मीद से उम्र
और छांव-छांव से पता
पूछना बेकार है।
(ये सीरीज जारी है)
 शिरीष खरे। स्वभाव में सामाजिक बदलाव की चेतना लिए शिरीष लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। दैनिक भास्कर , राजस्थान पत्रिका और तहलका जैसे बैनरों के तले कई शानदार रिपोर्ट के लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। संप्रति पुणे में शोध कार्य में जुटे हैं। उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
शिरीष खरे। स्वभाव में सामाजिक बदलाव की चेतना लिए शिरीष लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। दैनिक भास्कर , राजस्थान पत्रिका और तहलका जैसे बैनरों के तले कई शानदार रिपोर्ट के लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। संप्रति पुणे में शोध कार्य में जुटे हैं। उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।