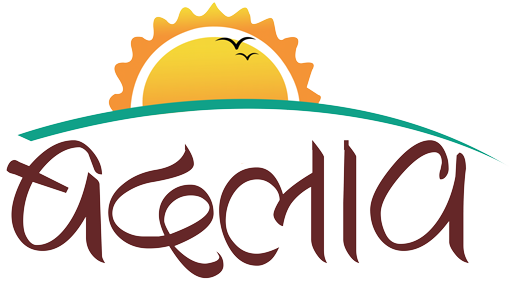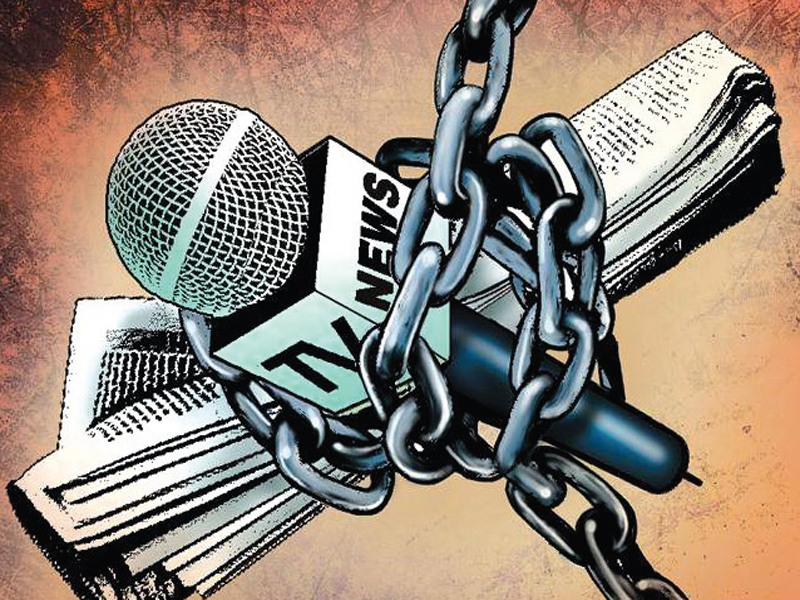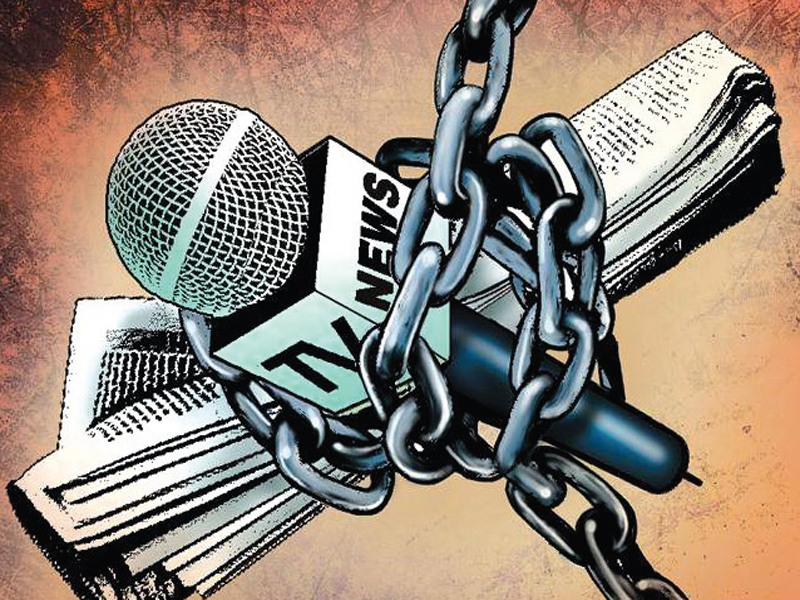 पुष्यमित्र
पुष्यमित्र
अमूमन ऐसे मौके कम ही आते हैं, जब पत्रकारों के संकट के बारे में बातें होती हैं। हालांकि पत्रकारिता का संकट इन दिनों जेरे-बहस है और इस देश में हर किसी की इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट राय है, मगर जो खतरा इस पत्रकारिता को संचालित करने वाली शक्ति यानी पत्रकारों पर है, उस पर बहुत कम लोगों की निगाह है। बमुश्किल डेढ़ दो साल पहले की बात है। उन दिनों मैं अपने अखबार के लिए घुमंतू रिपोर्टिंग करता था और इस दौरान अक्सर बिहार के जिलों और कस्बों के पत्रकारों से मिलना-जुलना और उनके घर आना जाना होता था। इसी सिलसिले में मैं बिहार के कोसी अंचल में अपने एक पत्रकार साथी के घर में था। हमलोग उनके दरवाजे पर बातें कर रहे थे कि तभी दो तीन बड़ी गाड़ियां रुकी और कुछ लोग गन लेकर उसके दरवाजे में घुसने लगे। साथी ने मुझे अंदर भेज दिया और कहा, बाहर मत आइयेगा।
दरवाजे से सटे कमरे में मैं बैठ गया, तभी उनकी पत्नी और उनके पिता भी उसी कमरे में आ गये। हम तीनों के कान इस बात को समझने में लगे थे कि बाहर हो क्या रहा है। गाड़ियों से आये लोग उस पत्रकार साथी से करीब आधे घंटे तक बहस करते रहे। बहस में गरमा-गरमी थी, अक्सर लगता था कि मारपीट की नौबत आ जायेगी। सामने वाले सज्जन पत्रकार साथी से कह रहे थे कि हम जब तुमको रेगुलर विज्ञापन देते हैं तो तुम हमारे खिलाफ खबर कैसे छाप सकते हो। पत्रकार साथी उसे बार-बार समझा रहे थे कि देखिये, विज्ञापन देने का मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी घटना हो जाये और हम उसकी खबर नहीं लिखें। दरअसल यह जो कहानी है, यह कोई रेयर कहानी नहीं है। देश के जिला और प्रखंड स्तर के कई पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, खास कर जो पत्रकार अपने उसूलों पर अडिग रहने की कोशिश करते हैं। सीवान में राजदेव रंजन की हत्या की जांच चल रही है और जांच का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है।
 इन तमाम अनुभवों से गुजरते हुए और लगातार जिलों और कस्बों के अपने पत्रकार साथियों से मिलते-बतियाते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे ये साथी आज की तारीख में एक अलग किस्म के खतरे का सामना कर रहे हैं और इसकी वजह इतनी सी है कि ये पत्रकार खबर लिखते के साथ-साथ अपने मीडिया हाउस के लिए विज्ञापन वसूलने का भी धंधा करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक ही आदमी किसी संस्थान के लिए विज्ञापन वसूले और जरूरत पड़ने पर विज्ञापन देने वाले के खिलाफ निगेटिव खबर लिखे तो सामने वाले उस व्यक्ति को सबक सिखाने के तरीके तलाशने लगता ही है। मगर मीडिया संस्थान इन पत्रकारों के खतरों से अनजान सिर्फ धन कमाने के लिए हर तरह के तिकड़म को अपनाने की कोशिश करते हैं। चाहे इसके लिए रिपोर्टर को विज्ञापन एजेंट या वितरक ही क्यों न बनाना पड़े।
इन तमाम अनुभवों से गुजरते हुए और लगातार जिलों और कस्बों के अपने पत्रकार साथियों से मिलते-बतियाते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे ये साथी आज की तारीख में एक अलग किस्म के खतरे का सामना कर रहे हैं और इसकी वजह इतनी सी है कि ये पत्रकार खबर लिखते के साथ-साथ अपने मीडिया हाउस के लिए विज्ञापन वसूलने का भी धंधा करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक ही आदमी किसी संस्थान के लिए विज्ञापन वसूले और जरूरत पड़ने पर विज्ञापन देने वाले के खिलाफ निगेटिव खबर लिखे तो सामने वाले उस व्यक्ति को सबक सिखाने के तरीके तलाशने लगता ही है। मगर मीडिया संस्थान इन पत्रकारों के खतरों से अनजान सिर्फ धन कमाने के लिए हर तरह के तिकड़म को अपनाने की कोशिश करते हैं। चाहे इसके लिए रिपोर्टर को विज्ञापन एजेंट या वितरक ही क्यों न बनाना पड़े।मैं बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय पत्रकारों की बात जानता हूं और मुझे लगता है कि देश के तकरीबन हर हिस्से में क्षेत्रीय पत्रकारों का यही हाल है। बिहार में 38 जिले और 534 प्रखंड हैं। चार बड़े सेंटर हैं जहां अखबारों ने अपने प्रिंटिंग सेंटर खोल रहे हैं। इन चार सेंटरों में काम करने वाले पत्रकारों को छोड़ दिया जाये तो बाकी जिलों के पत्रकारों को न अखबार ढंग की सैलरी देता है, न टीवी चैनल, पत्रिका और वेब पोर्टल तो आइकार्ड देकर पत्रकार बहाल कर लेते हैं। अखबार और क्षेत्रीय टीवी चैनलों के जिलों में जो संवाददाता होते हैं उनकी औसत सैलरी 5 से 8 हजार रुपये प्रति माह होती है और प्रखंडों-अंचलों में काम करने वाले पत्रकारों को मीडिया संस्थान 500 से 1500 रुपये के बीच प्रति माह मानदेय देते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने पैसे में इन पत्रकारों का घर नहीं चल सकता तो फिर इन्हें कहा जाता है कि ये मीडिया संस्थान के लिए विज्ञापन बुक करें और बदले में इन्हें हर विज्ञापन पर 10 से 20 फीसदी कमीशन मिलेगा।दुर्भाग्य से देश के ज्यादातर (फिल्ड में रहने वाले) पत्रकारों का जीवन इसी तरह चलता है।
 पत्रकारों के वेतन के निर्धारण के लिए समय-समय पर आयोग बनते थे। उसका काम सिर्फ कंपनियों के कंफर्म स्टाफ के वेतन का निर्धारण होता था, जो पूरी कंपनी का एक फीसदी भी नहीं होता था। 2011 में लागू हुए मजीठिया आयोग ने पहली दफा इन पत्रकारों की परेशानी कम करने का सुझाव दिया और निर्देश दिया कि प्रखंडों और जिलों में काम करने वाले पत्रकारों को प्रिंटिंग सेंटर में काम करने वाले पत्रकारों के लिए तय वेतन का क्रमशः 40 और 60 फीसदी मिला करे। क्योंकि अखबार इंडस्ट्री इन्हें पार्ट टाइम कर्मी मानती है।
पत्रकारों के वेतन के निर्धारण के लिए समय-समय पर आयोग बनते थे। उसका काम सिर्फ कंपनियों के कंफर्म स्टाफ के वेतन का निर्धारण होता था, जो पूरी कंपनी का एक फीसदी भी नहीं होता था। 2011 में लागू हुए मजीठिया आयोग ने पहली दफा इन पत्रकारों की परेशानी कम करने का सुझाव दिया और निर्देश दिया कि प्रखंडों और जिलों में काम करने वाले पत्रकारों को प्रिंटिंग सेंटर में काम करने वाले पत्रकारों के लिए तय वेतन का क्रमशः 40 और 60 फीसदी मिला करे। क्योंकि अखबार इंडस्ट्री इन्हें पार्ट टाइम कर्मी मानती है।इस लिहाज से प्रखंड के पत्रकारों का न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये और जिले वालों का 18 हजार रुपये होता। अगर ऐसा हो जाता तो काफी हद तक स्थिति सुधर जाती। मगर अखबार के मालिकों ने सरकार से मिलकर ऐसा खेल खेला कि सात साल बाद भी एक फीसदी पत्रकारों को भी इस वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला। अदालती खेल में पत्रकार बर्बाद हो गये। अखबारों ने झूठ का शोर मचा दिया कि अगर वह इस वेतन आयोग को लागू कर देती है तो अखबार चलाना मुश्किल हो जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद लेबर कोर्ट के पाले में डाल दिया।
सरकारी विज्ञापन नीति का पत्रकारिता पर खास असर है। बिहार की बात करें तो यहां मुख्य रूप से चार बड़े अखबार प्रकाशित होते हैं। इन अखबारों की आय में 40 से 50 फीसदी हिस्सा सरकारी विज्ञापनों का होता है। दूसरे राज्यों में यह हिस्सा कम होता होगा, मगर इतना नहीं कि इसे इग्नोर किया जा सके।बिहार जैसे राज्य में इन विज्ञापनों का महत्व आप समझ ही सकते हैं। इस साल मैंने खास तौर पर इस बात पर गौर किया कि इनमें से तकरीबन सभी अखबारों को जारी होने वाले विज्ञापन सरकार बीच-बीच में बंद कर देती है। इनका एक पैटर्न है, जो अखबार सरकार को चुभने वाली खबर का प्रकाशन करता है, उसे विज्ञापन जारी होना बंद हो जाता है। दस-पंद्रह दिन बाद अखबार का प्रबंधन सरकार के दरबार में चक्कर काटते दिखते हैं और इस मुलाकात के बाद सरकार को खुश करने के लिए सरकार के समर्थन वाली खबरें छपने लगती हैं । फिर एक दिन विज्ञापन शुरू हो जाता है। दिलचस्प है कि सरकार किसी खोजी खबर से ही नाराज नहीं होती, वह तो अब छपना भी बंद हो गया है। किसी हार्ड न्यूज से भी अगर सरकार की छवि खराब होती हो, तो सरकार उससे भी नाराज हो सकती है। इसलिए ऐसी खबरों को अंदर के पन्ने पर प्रकाशित करने का चलन शुरू हो गया है।
ऐसा पहले नहीं था, पहले विज्ञापन जिले के स्तर से जारी होते थे। इसके अलावा नगर निगम, विवि और अलग-अलग सरकारी संस्थान और राज्य के विभिन्न मंत्रालय अलग-अलग विज्ञापन जारी करते थे। मगर कुछ साल पहले सरकार ने तमाम विज्ञापनों का केंद्रीकरण कर दिया। पहले जब अलग-अलग विज्ञापन जारी होते थे, तो इतनी परेशानी नहीं होती थी। एक विभाग का मूड खराब हुआ तो दस देने वाले होते थे। मगर जब से केंद्रीकरण हुआ है, एक आदमी के मूड पर तमाम विज्ञापन निर्भर हैं।
और यह विज्ञापन नीति अखबारों को लगातार कमजोर, रीढ़ विहीन और पंगु बना रही है। इसलिए अगर पत्रकारिता को बचाना है तो हमें खास कर इस मसले पर आवाज उठानी होगी।
 पुष्यमित्र। पिछले डेढ़ दशक से पत्रकारिता में सक्रिय। गांवों में बदलाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर आपकी पैनी नज़र रहती है। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता का अध्ययन। व्यावहारिक अनुभव कई पत्र-पत्रिकाओं के साथ जुड़ कर बटोरा। संप्रति- प्रभात खबर में वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी। आप इनसे 09771927097 पर संपर्क कर सकते हैं।
पुष्यमित्र। पिछले डेढ़ दशक से पत्रकारिता में सक्रिय। गांवों में बदलाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर आपकी पैनी नज़र रहती है। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता का अध्ययन। व्यावहारिक अनुभव कई पत्र-पत्रिकाओं के साथ जुड़ कर बटोरा। संप्रति- प्रभात खबर में वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी। आप इनसे 09771927097 पर संपर्क कर सकते हैं।