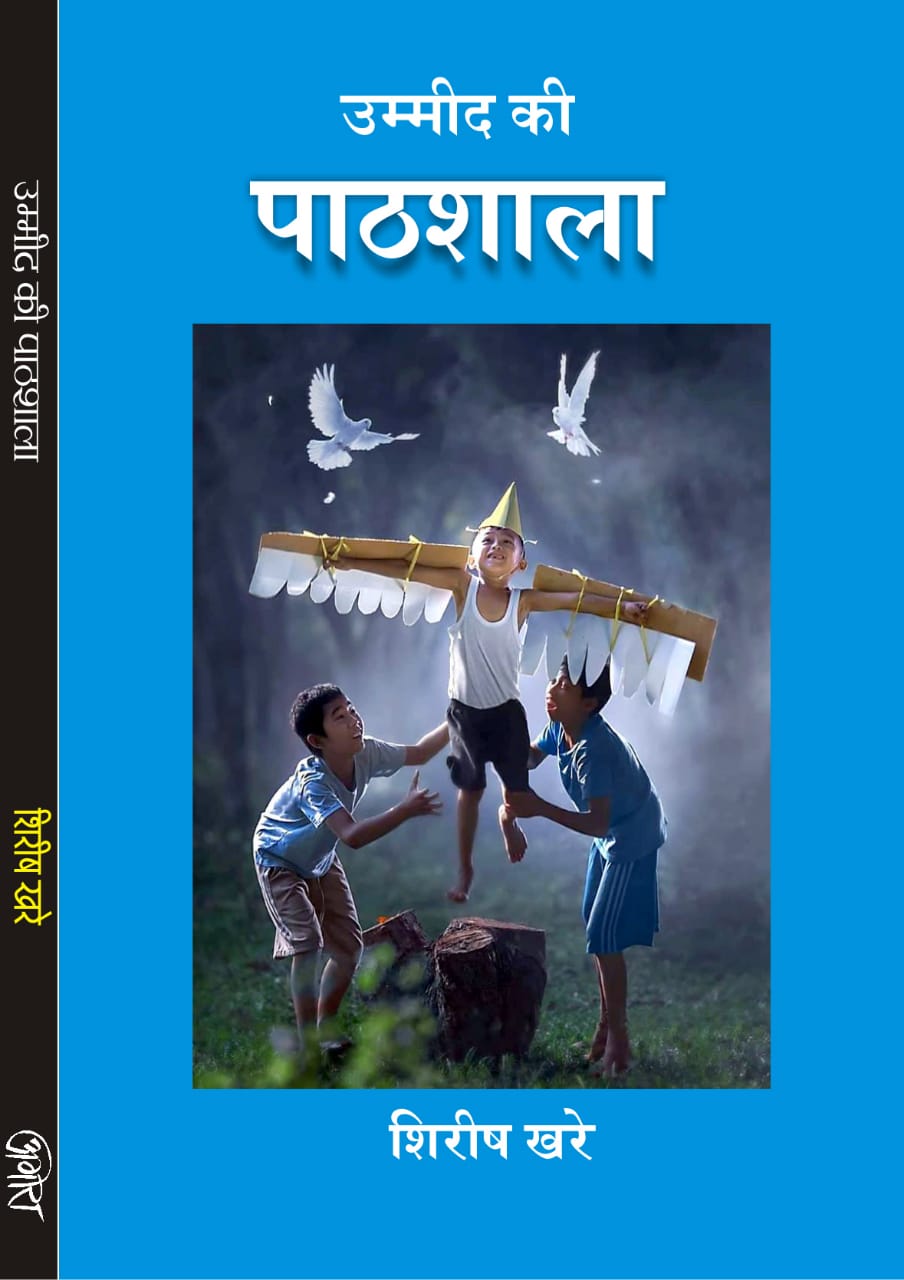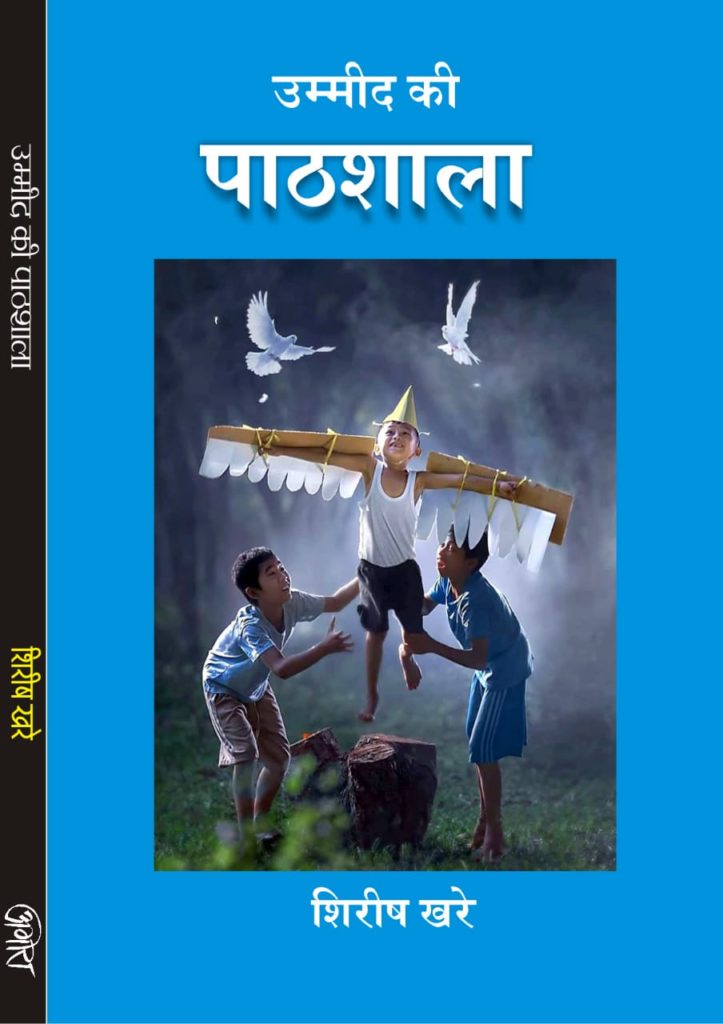
बरुण सखाजी
ढहते सरकारी स्कूलों में से उम्मीदें खोजती शिरीष खरे की “उम्मीद की पाठशाला” शिक्षा क्षेत्र की अहम किताब है। वे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान के स्कूलों में घूमती साक्षात् दृष्टि के रूप में प्रकट हैं। “उम्मीद की पाठशाला” उस दौर की अहम किताब है, जब सरकारी स्कूलों में अध्ययन गरीबी या बेबसी का प्रतीक बन चुका है। ऐसे वक्त में इस बिखरते सिस्टम को संवारना आवश्यक है। किताब किसी पॉलिसी चेंज की कोई वकालत नहीं करती, न किसी अधोसंरचनागत बदलाव की अपेक्षा करती। यह निःशर्त इन स्कूलों में सकारात्मकता देखती है।
“उम्मीद की पाठशाला” उन शिक्षकों के लिए भी उम्मीद है जो कहीं किसी कोने के स्कूल में अच्छा काम करने की प्रेरणा तो रखते हैं, जज्बा भी उनमें है, परंतु इसे पहचान नहीं मिल पाती। इस किताब में ऐसे 50 से अधिक शिक्षकों और शिक्षकों के समूहों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जो अपनी भूमिकाएं सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखते। एक दौर में स्कूल शिक्षक गांवों में श्रद्धा का केंद्र हुआ करता था। उसके कंधे पर सिर्फ पढ़ाई का दायित्व नहीं था, बल्कि जीवन बनाने की जिम्मेदारी थी। उस वक्त न कोई प्रशासनिक इतनी मॉनटरिंग न कोई कथित कसावट। शिक्षक सम्मानपूर्वक अपना दायित्व निभाता और नतीजे में कोई ही बच्चे विफल होते। लेकिन कालांतर में अर्थव्यवस्था से संचालित होने वाले जीवन में शिक्षक की यह मूर्ति ढहा दी गई। संविदा, वेतन की सब्जी-भाजी खरीदने जैसी वार्गेनिंग, हकों के लिए सड़कों पर उतरने को विवश शिक्षक, पोलियो दवा से लेकर जनसंख्या तक में उलझे शिक्षकों के पास अपने कोर कार्य कम ही बचे। ऐसे में सरकारी स्कूलों के ढहने की वजह सिर्फ निजी स्कूल नहीं, न सरकार की शिक्षानीति, बल्कि प्रेरणा का अभाव है।

“उम्मीद की पाठशाला” यही प्रेरणा खोजती है। पुस्तक में दो दर्जन से अधिक सरकारी स्कूलों के ऐसे काम हैं जिनमें सबकी प्रेणा से नए ढंग से काम किए गए। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा हो, नक्सल प्रभावित बस्तर हो या रायपुर के पास ही में शहरी दायरे का सरकारी स्कूल। सबकी कहानी रोचक ढंग से पेश की गई है। यहां के शिक्षकों के मनोबल, कार्य की प्रेणा और सकारात्मक दृष्टिकोण को समझा गया है। अकालग्रस्त मराठवाड़ा में कैसे लाठागांव के बच्चों ने पढ़ाई के अलावा पेड़ों की श्रृंखला खड़ी कर दी। पेड़ों में पानी के लिए कैसे एक शिक्षक की प्रेरणा से कइयों लीटर पानी जुटता और पेड़ गर्मियों में भी सिंचित होते रहे। इस पानी प्रबंधन में बच्चों ने गणित भी सीखा। हर बच्चे को एक बोतल पानी घर से लाना होता, कुल कितने बच्चे, कितनी बोतल, कितना पानी गया पेड़ को आदि तकनीकी से गणित के साथ पर्यावरण बचाओं की प्रेरणा का युग्म काबिले तारीफ है। यही प्रेरणा महाराष्ट्र के पालघर जिले के स्कूलों में भी देखने को मिलती।
गोवा के पणजी का वह स्कूल जहां बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया जाता है। 8 मार्च के खास दिन यहां के भावुक माहौल का जिक्र बड़ा अच्छा है। वहीं गोवा के ही बिचोलम तहसील पणजी के पास का वह स्कूल भी रोचक कार्य कर रहा है, जहां आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को वीडियो के जरिए पढ़ाया जाता है। पणजी के पास ही गांव शिरगाव की कहानी भी रोचक है, जहां प्लास्टिक मुक्ति का जिम्मा बच्चों ने अपने कंधों पर लिया। समुदी तट पर भारी प्लास्टिक देख दुखी बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर इतनी बड़ी मुहिम शुरू कर दी। यहां यह वाक्य सटीक सिद्ध होता है “पहले करो फिर कहो”।

चीनी मिलों के लिए मशहूर उम्मानाबाद महाराष्ट्र की कहानी भी बड़ी रोचक और जज्बाती है। यहां मजदूरों के जीवन और शिक्षा की उम्मीद के किस्से हैं। इस दौरान शिरीष की वह लाइन जिम्मेदारी का अहसास कराती है कि यहां मजदूरों के बीच रिश्ते भी एक की बजाए दो हाथ होंगे कमाने वाले के आधार पर बनते हैं। इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा बलवती है। चूंकि 10 साल की उम्र के बच्चे बोझा ढोने वाले कार्यो में जुट जाते हैं, 14-15 तक आत-आते वे जीवन संग्राम में एक वयस्क के समान काम करने लगते हैं। कानूनों की बात करें तो वे अपना पेट भी न भर पाएं। लाख योजनाओं के बाद भी इनकी माली हालत नहीं सुधर पाती।
वहीं कुछ ऐसे स्कूलों की कहानी भी दमदार है, जहां भाषाई सीमाएं पार करने के लिए शिक्षकों ने युक्ति लगाई। कहीं चित्रों से बात की गई कहीं प्रतीकों के जरिए। कई स्कूलों में 6 किलोमीटर दूर से आने वाले संघर्षशील बच्चों की कहानी है, तो कहीं छत्तीसगढ़ के दिल्ली साब के समर्पित जीवन का किस्सा। युक्तियुक्तकरण के नाम पर अनुपयुक्त रूप से बंद किए गए स्कूलोंं के किस्से भी इस पुस्तक में हैं। दंतेवाड़ा के घने जंगलों में एक तरफ माओवादी स्कूल इमारतें ढहा देते हैं तो दूसरी तरफ सरकार स्कूल बंद कर रही है। ऐसे में ज्योति का प्रकाश बन रहे हैं यहां के बच्चे और स्कूल शिक्षक। “उम्मीद की पाठशाला” बड़े सधे ढंग से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों के शिक्षकों की भर्ती पर भी बात करती है।
किताब की अच्छी कहानी है पारिधी जनजाति के स्कूल की। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक गांव इनका है। अंग्रेजों के जमाने से चोरी के लिए चिन्हित की गई इस जनजाति में पुलिस को लेकर भय है। यहां एक सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर काफी मिथ टूट रहे हैं। आदिवासी अंचलों में बसे गांव और वहां के स्कूलों में बड़े काम हो रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ के बद्रीडांड गांव के रेवाराम की कहानी, यहीं के केरवा गांव की दिलेश्वरी की कहानियां रोचक हो सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर ऐसा है कि कई निजी स्कूल बंद हो गए। रायपुर के पास डूमरतराई में एक स्कूल ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त है। महासमुंद का स्कूल जहां हाईटेक तरीके से पढ़ाई होती है। “उम्मीद की पाठशाला” इन सब पर लंबी बात करती है।

बांधों से प्रभावित गांव, संस्कृति और शिक्षा पर नर्मदा की जीवन शाला रोचक वृतांत है। विस्थापन को शिरीष ने सधे ढंग से कहा है… “दोबारा बार-बार बसना, सरकारी योजना का लाभ न उठा पाना, कानून हक न मिलना, मेजबान समुदाय की आनाकानी, नया समायोजन, शोषण, यौन उत्पीड़न, अधिक व्यय, हिंसा, अपराध, अव्यवस्था, संसाधन, सीमित जमीन, निर्णय की गतिविधि से कटाव, अस्थायी मजदूरी, मवेशियों का त्याग, प्रदूषण, सुविधा व स्वास्थ्य संकट।” सरदार सरोवर बांध की जद में आने वाली जमीन पर बसे लोगों की बोलियों में शिरीष कुछ अच्छी कहानियों का भी जिक्र करते हैं। अमरीकन शिक्षिका जूलिया वेबर की 30 के दशक की किताब और हेमराज की डायरी का मिश्रण अद्भुत है।
“उम्मीद की पाठशाला” प्रधानमंत्री की मन की बात के बेहद करीब है। वे भी अपने इस कार्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज और सकारात्मकता की बात करते हैं।
शिरीष ने अपनी किताब उम्मीद की पाठशाला में गांवों में संचालित स्कूलों की सकारात्मकता के लिए जो कोशिश की है इस पर सिर्फ वाह-वाह करने से अच्छा होगा कि राज्य की सरकारें सरकारी स्कूलों की इमेज बिल्डिंग के लिए मुकम्मल तौर पर काम करें। कायदों और कानूनों से उत्थान में बहुत वक्त लगेगा। अधोसंचरना विकसित करने की बात होगी तो और भी अधिक समय और धन लगेगा, लेकिन जो है जैसा है वैसे में ही कुछ प्रेरक किया जाने लगे तो बात बन सकती है।
“उम्मीद की पाठशाला” पढ़ने के बाद दो ख्याल आते हैं, पहला तो सरकारी स्कूलों की हालत जितनी खराब है वह तो है ही, परंतु इनका नैतिक, मानसिक मनोबल जितना गिरा है वह घातक है। अगर राज्य की ओर से स्कूलों के बीच विभिन्न गतिविधियों के जरिए ग्मैरस रैंकिंग और अवार्ड किए जाने लगें तो हालात काफी कुछ सुधर सकते हैं। कम से कम उनके पास तो करने को होगा जो करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि स्कूल, शिक्षा, कॉलेज, विश्वविद्यालय पर भारत में कोई मुकम्मल पत्रकारिता नहीं होती। पार्ट-पार्ट में जिसे जो मिला वह छापा, पुरस्कार लिए और काम खत्म जैसे हाल हैं। यहां शिक्षा पर बहुत संकुचित दृष्टि से देखा, समझा, सुना जा रहा है। ब्रह्मकुमारीज आध्यात्मिक संस्था से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित अक्सर कहा करते हैं, अखबार में एक खबर प्रेरणा की होनी चाहिए। किसी ऐसे अनसंग हीरोज को समाज से जरूर रुबरु करवाना चाहिए जिसे पढ़कर लोगों में चेतना जागृत हो। शिरीष खरे की यह पहल इस बात के इर्दगिर्द एक अच्छी है।
“उम्मीद की पाठशाला” को अमेजन से मंगवाया जा सकता है। इसे अगोरा प्रकाशन बनारस ने छापा है।