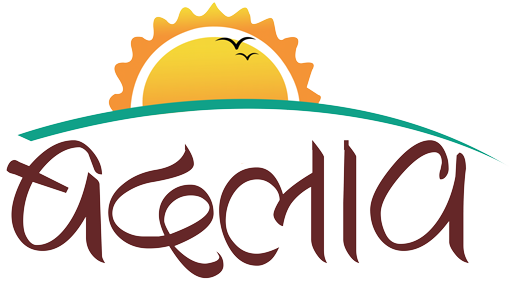डॉक्टर गंगा सहाय मीणा
 देश के तमाम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुलपति, एकेडमिशियन, आलोचक, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक इसी देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों से निकले हैं। संख्या में कम ही सही, लेकिन सरकारी अनुदान से चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान सीमित संसाधनों में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे संस्थानों में आईआईटी, आईआईएससी, एम्स, जिपमर, पीजीआई, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एचसीयू आदि प्रमुख हैं।
देश के तमाम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुलपति, एकेडमिशियन, आलोचक, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक इसी देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों से निकले हैं। संख्या में कम ही सही, लेकिन सरकारी अनुदान से चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान सीमित संसाधनों में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे संस्थानों में आईआईटी, आईआईएससी, एम्स, जिपमर, पीजीआई, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एचसीयू आदि प्रमुख हैं।पिछले वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है कि ज्यादातर कैंपस उबाल पर हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जेएनयू- सभी महत्वपूर्ण कैंपसों में छात्रों और अध्यापकों ने अपने एकेडमिक अधिकारों के लिए आंदोलन किये हैं। अभी यूजीसी-मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नए आदेश से इनमें से अधिकांश संस्थानों को ‘स्वायत्त’ किया जा रहा है। सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से मुखातिब होते वक्त बताया कि कुछ 60 संस्थानों को स्वायत्त किया जा रहा है। इन संस्थानों का चुनाव नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) रैंकिंग के आधार पर किया गया है। यानी जो देश में सबसे अच्छे संस्थान हैं, उन्हें स्वायत्तता दी जा रही है।
 जावड़ेकर जी ने स्वायत्तता के मायने बताते हुए कहा कि अब इन संस्थानों को नए कोर्स बनाने, नए विभाग शुरू करने, नए कैंपस बनाने, नियुक्तियां करने आदि के लिए यूजीसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। न ही यूजीसी इनका निरीक्षण करेगी। ये संस्थान दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से मनमानी तनख्वाह देकर फैकल्टी भी बुला सकेंगे और मनमानी फीस लेकर विदेशी विद्यार्थी भी भर्ती कर सकेंगे। जावड़ेकरजी ने प्रेस बयान में मुख्यतः एकेडमिक स्वायत्तता के बारे में बात की जबकि इस आदेश के मूल में आर्थिक स्वायत्तता ही नज़र आ रही है। बेहतरीन शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता की आड़ में निजी हाथों में सौंप देने संबंधी ज्ञान आयोग और नीति आयोग की सिफारिशों पर 2017 से अमल किया जाना शुरू हो गया था। ड्राफ्ट बनाया गया, राय मांगी गई और अंततः 12 फरवरी 2018 को गजट नोटिफिकेशन निकालकर विश्वस्तरीय गुणवत्ता के आवरण में इस स्वायत्ता संबंधी आदेश को लागू कर दिया गया।
जावड़ेकर जी ने स्वायत्तता के मायने बताते हुए कहा कि अब इन संस्थानों को नए कोर्स बनाने, नए विभाग शुरू करने, नए कैंपस बनाने, नियुक्तियां करने आदि के लिए यूजीसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। न ही यूजीसी इनका निरीक्षण करेगी। ये संस्थान दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से मनमानी तनख्वाह देकर फैकल्टी भी बुला सकेंगे और मनमानी फीस लेकर विदेशी विद्यार्थी भी भर्ती कर सकेंगे। जावड़ेकरजी ने प्रेस बयान में मुख्यतः एकेडमिक स्वायत्तता के बारे में बात की जबकि इस आदेश के मूल में आर्थिक स्वायत्तता ही नज़र आ रही है। बेहतरीन शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता की आड़ में निजी हाथों में सौंप देने संबंधी ज्ञान आयोग और नीति आयोग की सिफारिशों पर 2017 से अमल किया जाना शुरू हो गया था। ड्राफ्ट बनाया गया, राय मांगी गई और अंततः 12 फरवरी 2018 को गजट नोटिफिकेशन निकालकर विश्वस्तरीय गुणवत्ता के आवरण में इस स्वायत्ता संबंधी आदेश को लागू कर दिया गया।20 मार्च को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत इस आदेश में जिस एकेडमिक स्वायत्तता की बात की गई है, उन सबके अंत में एक बात लिखी हुई है- इसके लिए फंड सरकार नहीं देगी, स्वयं जुटाना होगा। यानी अगर इन संस्थानों में से किसी संस्थान को कोई नया कोर्स शुरू करना है तो वह कर सकता है, बशर्ते इसके लिए फंड वह खुद जुटाए। 12 फरवरी के गजट आदेश में इस तरह की तमाम बातें विस्तार से दर्ज हैं। इसलिए इसका विरोध भी आने के साथ ही शुरू हो गया। 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 70-30 फॉर्मूला लागू करने के प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वहां के शिक्षक आंदोलनरत हैं। एकेडमिशियनों का सोचना है कि ये सारी कोशिशें शिक्षा के निजीकरण के लिए चल रही मुहिम का हिस्सा है।
भारत में निजीकरण की बयार 1990 के आसपास से शुरू हुई जो लगातार तेज होती चली जा रही है। अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उदारवादी और नवउदारवादी नीतियों के तहत तेजी से निजीकरण हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा- तीनों स्तरों पर सरकारी शिक्षण संस्थान नाममात्र रह गए हैं। मौजूदा आदेश से लगता है कि अब बचे हुए संस्थानों से भी सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है।
 जिस स्वायत्तता की बात सरकार कर रही है उसके बाद विश्वविद्यालयों के कोर्सों के स्वरूप, प्रवेश प्रक्रिया, स्कॉलरशिप, फैलोशिप, मूल्यांकन, फीस आदि से यूजीसी की निगरानी खत्म हो जाएगी। संस्थान मनमर्जी के कोर्स बनाएंगे और मनमाफिक फीस लेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ज्योतिष और कर्मकांड जैसे कोर्स प्रस्तावित किये गए थे, जिन्हें देश के एकेडमिशियनों ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब अगर किसी विश्वविद्यालय ने कोई कोर्स बना लिया तो उसे चलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वायत्त विश्वविद्यालय, उनके कैंपस और कॉलेज यूजीसी से स्वतंत्र हो जाएंगे। उनकी सरकार और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी। जब सरकार फंड नहीं करेगी तो कौन करेगा? जाहिर है निजी पूंजी निवेश शुरू होगा और उनकी रुचि और आवश्यकतानुसार कोर्स और फीस निर्धारित की जाएगी। अकादमिक राय की जगह बाजार की राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्रमशः शिक्षा अपने मूल लक्ष्यों- विचार, समानता और लोकतंत्र निर्माण से दूर होती चली जाएगी।
जिस स्वायत्तता की बात सरकार कर रही है उसके बाद विश्वविद्यालयों के कोर्सों के स्वरूप, प्रवेश प्रक्रिया, स्कॉलरशिप, फैलोशिप, मूल्यांकन, फीस आदि से यूजीसी की निगरानी खत्म हो जाएगी। संस्थान मनमर्जी के कोर्स बनाएंगे और मनमाफिक फीस लेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ज्योतिष और कर्मकांड जैसे कोर्स प्रस्तावित किये गए थे, जिन्हें देश के एकेडमिशियनों ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब अगर किसी विश्वविद्यालय ने कोई कोर्स बना लिया तो उसे चलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वायत्त विश्वविद्यालय, उनके कैंपस और कॉलेज यूजीसी से स्वतंत्र हो जाएंगे। उनकी सरकार और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी। जब सरकार फंड नहीं करेगी तो कौन करेगा? जाहिर है निजी पूंजी निवेश शुरू होगा और उनकी रुचि और आवश्यकतानुसार कोर्स और फीस निर्धारित की जाएगी। अकादमिक राय की जगह बाजार की राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्रमशः शिक्षा अपने मूल लक्ष्यों- विचार, समानता और लोकतंत्र निर्माण से दूर होती चली जाएगी।जिन संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया है, उनमें से अधिकांश में विद्यार्थियों से बहुत ही कम फीस ली जाती है। वह इसलिए नहीं कि उनकी पढाई पर खर्च कम आता है, बल्कि इसलिए कि उनका खर्च सरकार उठाती है। एक समाजवादी लोककल्याणकारी राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराए। जब इन बेहतरीन शिक्षण संस्थानों को सरकारी मदद कम या बंद हो जाएगी, निश्चित तौर पर रियायतों में कटौती होगी और फीसों में बढोतरी। इससे सामाजिक न्याय की योजनाएं भी प्रभावित होंगी।
यह भी अजब संयोग है कि इसी महीने यूजीसी का नया रोस्टर नियम भी आया है जिसके बाद विश्वविद्यालयों की नौकरियों में समाज के वंचित तबकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो जाएगा। ये दोनों आदेश उच्च शिक्षा के समाजवादी लोकतांत्रिक स्वरूप को गंभीर आघात पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों के शिक्षक इनके खिलाफ आंदोलनरत हैं। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा में तमाम तबकों की भागीदारी बढाने के लिए जहां और बेहतरीन सरकारी संस्थानों की आवश्यकता है, वहां सरकार द्वारा अच्छा कर रहे शिक्षण संस्थानों के निजीकरण के लिए दरवाजे खोलना निराशाजनक है। अगर शिक्षा के रास्ते विचारों पर बाजार का कब्जा हो गया तो डर है कि धीरे-धीरे वह पूरे लोकतंत्र को ही गुलाम बना लेगा।