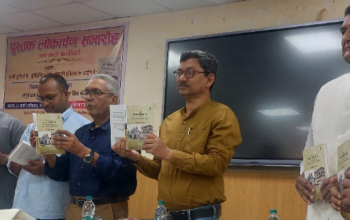ब्रह्मानंद ठाकुर
जाने – माने समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा की पुस्तक ‘ गांधी और व्यावहारिक अराजकवाद ‘ की शृंखला की तीसरी कड़ी में गांधी और कतिपय अराजकवादी विचारकों के वैचारिक द्वन्द्व की चर्चा की गई थी। कुछ बिन्दुओं पर दोनों के विचारों में समानता भी है लेकिन ,जो बातें गांधी की सोच को अराजकवादियों या तथिकथित यूटोपियाई समाजवादियों की सोच के नजदीक लाती है, वह शायद मनुष्य मात्र के अचेतन में दबी उनमुक्त जीवन की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। आज प्रस्तुत है शृंखला की चौथी कड़ी।

हमारे आदिम पूर्वज कभी घने वनों में छोटे समूहों में पारस्परिक सहयोग के आधार पर जीते थे। उनकी आवश्यकता के हिसाब से संसाधनों की सहज उपलब्धता थी। उस जीवन के प्रतिमान शायद आज भी हमारे जीन में उपस्थित हैं, हालांकि हमारे जीवन की स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अदन के बाग का उनमुक्त जीवन, न्यू अटलांटिस, सतयुग या यूटोपिया की तलाश कहीं न कहीं हमारी उस आदिम व्यवस्था की चाहत की ही अभिव्यक्ति है। समता और सामुदायिकता की तलाश हमारे घोर व्यक्तिवादी समाज के दबावों के बाबजूद खत्म नहीं होती।

एथोलाजिस्ट डेस्मंड मारिस ने अपनी चर्चित पुस्तक ‘ ‘द ह्यूमनमन जू’ में लिखा है कि आज के निर्वैयक्तिक समाज में, जहां लाखों लोगों को साथ रहना होता है वहां भी प्रत्येक व्यक्ति पुराने जैविक किस्म का वैयक्तिक संबंध कबीलाई आकार के छोटे पेशागत या सामाजिक समूह के साथ स्थापित कर लेता है। इस छोटे समूह में वह स्वभाव में निहित पारस्परिक सहयोग और सम्पत्ति साझा करने के रुझान को तुष्ट कर सकता है। मानव समाज में अंतर्निहित सामुदायिकता विषमतामूलक समाज के विकास के क्रम में उसके, अचेतन में दबा दी गई है। लेकिन विशेष अवसरों पर यह फिर उसकी चेतना में उभर आती है। गांधी जी के जीवन मे इस तरह का बदलाव रस्किन की पुस्तक ‘अन टू दिस लास्ट ‘ पढने के बाद आया और उसी क्षण से वे मानो साम्यवादी बन गये- महज दिमागी अय्याशी के लिए नहीं , व्यावहारिक जीवन में।
गांधीजी के अनुसार सिद्धांत रूप में पुस्तक अन टू द लास्ट का निष्कर्ष था :1. व्यक्ति की भलाई सबों की भलाई में निहित है। 2.एक वकील के काम का वही महत्व है जो एक नाई के काम का , क्योंकि सबों को अपने काम से आजीविका पाने का अधिकार है। 3. श्रम का जीवन , यानि एक हलवाहे का जीवन जो जमीन जोतता है एवं एक दस्तकार का जीवन जीने योग्य है। इस नतीजे पर पहुंचने के साथ ही गांंधीजी ने सामुदायिक श्रम पर आधारित जीवन की शुरुआत अपनी पत्रिका ‘इण्डियन ओपिनियन ‘ के प्रकाशन की नई व्यवस्था से की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास फीनिक्स में जमीन खरीद कर अपने भारतीय और यूरोपीय सहयोगी के साथ सामूहिक श्रम के आधार पर आवास निर्माण से लेकर प्रेस चलाने तक का सारा काम खुद किया। इसमें सम्पादक और श्रमिक सबकी समान सहभागिता थी। यह बिना किसी राज्य व्यवस्था के नियंत्रण या सहयोग के स्वावलम्बन पर आधारित सामुदायिक श्रम का प्रयोग था। इस क्रम में एक समय ऐसा भी आया जब इन लोगों ने मशीन की जगह अपने शारीरिक श्रम से ही प्रेस को चलाना शुरू कर दिया और गांधीजी ने जैसा लिखा है , उनके लिए वे नैतिक उत्थान के सर्वोच्च क्षण थे।
सामुदायिक जीवन का इससे भी बड़ा प्रयोग टाल्सटाय फार्म का था। यह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे भारतीयों के परिवारों की आजीविका की व्यवस्था के लिए किया गया। इसमें जेल की सजा काट रहे सत्याग्रहियों के परिवारों के सामूहिक जीवन की व्यवस्था की गई थीः शुरू में इसमें दस औरतों और सात मर्दों के लिए व्यवस्था की गई। इसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। इसके अलावा इसमें तमिल, तेलगु, गुजराती और उत्तर भारतीय थे। अपने लिए आवास का निर्माण सब ने मिल कर स्वयं किया था। भाषाई भिन्नता के बावजूद इनकी शिक्षा की सम्मिलित व्यवस्था की गई थी। मल – मूत्र आदि के निस्तार की ऐसी व्यवस्था की गयी, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और साथ ही उपयोगी खाद तैयार हो जाए, जो सामुदायिक कृषि के लिए उपयोग में आये।
यह सब होना चमत्कार -सा लगेगा जबतक हम यह न मान लें कि सहयोग और पारस्पारिकता का भाव मनुष्य का आनुवंशिक गुण है , जिसे प्रतिस्पर्धा की वर्तमान सभ्यता ने हजारों वर्ष के विकास के क्रम में नष्ट करने का काम किया है। संघर्ष के साथ रचना का कार्यक्रम , जो गांधीजी के आंदोलन का महत्वपूर्ण चरित्र रहा है, उस दिशा की ओर इशारा करता है, जिस दिशा में चलकर वर्तमान सभ्यता के विकल्प में इसके भीतर से ही एक नयी जीवन पद्धति का विकास किया जा सकेगा। अराजकवादियों की यह कल्पना कि किसी तरह धक्का देकर वर्तमान व्यवस्था को नष्ट कर देने से सहयोग आधारित समाज स्वत: अस्तित्व में आ जाएगा, किसी चमत्कार की आशा जैसी लगती है।
1960 के दशक में फ्रांस से शुरू हो यूरोप अमेरिका में छात्रों का आंदोलन और बाद में इसके समर्थन में जुड़े मजदूरों का निषेध पक्ष तो प्रखर था जिसने औद्योगिक व्यवस्था के स्थापित मूल्यों ( प्रतिस्पर्धा एवं युद्ध ) के विनाशकारी चरित्र को उजागर किया। लेकिन किसी विकल्प के अभाव में उस समय का विद्रोही युवा पुराने ढांचे को ही स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। आधी शताब्दी बाद उन आंंदोलनों की स्मृति भी शेष नहीं रही। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता हर स्तर पर मजदूरों के शोषण से लेकर पर्यावरण के विरुद्ध अनियंत्रित आक्रमण पर आधारित है। खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के लिए धरती की चट्टानी सतहों की तोड़-फोड़, वनों की कटाई, जलस्रोतों का अतिशय दोहन और नदियों से लेकर भूगर्भ जलस्रोतों तक के जल को रासायनिक कचड़ों से प्रदूषित करना प्रकृति विरोधी हिंसा के आयाम हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ हुई सभी क्रांतियां अंंतत; इसी हिंसात्मक संस्कृति का हिस्सा बन कुछ फेरबदल के साथ इसी व्यवस्था को चलाने में लगी रही है।

ब्रह्मानंद ठाकुर।बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के निवासी। पेशे से शिक्षक। मई 2012 के बाद से नौकरी की बंदिशें खत्म। फिलहाल समाज, संस्कृति और साहित्य की सेवा में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर के पियर गांव में बदलाव पाठशाला का संचालन कर रहे हैं।